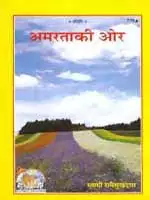|
गीता प्रेस, गोरखपुर >> अमरता की ओर अमरता की ओरस्वामी रामसुखदास
|
412 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है अमरता की ओर...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
निवेदन
प्रस्तुत पुस्तक में परमश्रद्धेय श्रीस्वामीजी महाराज के नौ लेखों का
संग्रह है। पारमार्थिक रुचिवाला प्रत्येक साधक इनका अध्ययन-मनन करके
मृत्यु से ऊँचा उठकर अमरता प्राप्त कर सकता है। परन्तु साधक का उद्देश्य
अनुभव करने का होना चाहिये, कोरी बातें सीखने का नहीं सीखा हुआ ज्ञान
अभिमान बढ़ाने के सिवाय और कुछ काम नहीं आता। अतः पाठकों से निवेदन है कि
वे अनुभव करने के उद्देश्य से इस पुस्तक का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन-मनन
करें और अपना मानव-जीवन सार्थक करें
-प्रकाशक
1. अमरता का अनुभव
मनुष्यता के भीतर स्वाभाविक ही एक ज्ञान अर्थात् विवेक है। साधक का काम उस
विवेक को महत्त्व देना है। वह विवेक पैदा नहीं होता। अगर वह पैदा होता तो
नष्ट भी हो जाता; क्योंकि पैदा होनेवाली हरेक चीज नष्ट होनेवाली होती
है—यह नियम है। अतः विवेक की उत्पत्ति नहीं होती, प्रत्युत
जागृति
होती है। जब साधक अपने भीतर उस स्वतःसिद्धि विवेक को महत्त्व देता है, तब
वह विवेक जाग्रत हो जाता है। इसी को तत्त्वज्ञान अथवा बोध कहा जाता है।
मनुष्यतामात्र के भीतर स्वतः यह भाव रहता है कि मैं बना रहूँ, कभी मरूँ नहीं। वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। अगर वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। जैसे, भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु (अन्न और जल) है, जिससे वह भूख-प्यास बुझ जाय। अगर अन्न-जल न होता तो भूख-प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतःसिद्ध है। यहाँ शंका होती है कि जो अमर है, उसमें अमरता की इच्छा क्यों होती है ? इसका समाधान है कि अमर होते हुए भी जब उसने अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्म शरीर के साथ अपने को एक मान लिया अर्थात् ‘शरीर ही मैं हूँ’—ऐसा मान लिया, तब उसमें अमरता की इच्छा और मृत्यु का भय पैदा हो गया।
मनुष्य मात्र को इस बात का विवेक है कि यह शरीर (स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर) मेरा असली स्वरूप नहीं है। शरीर प्रत्यक्ष रूप से बदलता है। बाल्यावस्था में जैसा शरीर था, वैसा आज नहीं है और आज जैसा शरीर है, वैसा आगे नहीं रहेगा। परन्तु मैं वही हूँ अर्थात् बाल्यवस्था में जो मैं था, वही मैं आज हूँ और आगे भी रहूँगा। अतः मैं शरीर से अलग हूँ और शरीर मेरे से अलग है अर्थात् मैं शरीर नहीं हूँ—यह सबके अनुभव की बात है। फिर भी अपने को शरीर से अलग न मानकर शरीर के साथ एक मान लेना अपने विवेक का निरादार है अपमान है, तिरस्कार है। साधक को अपने इस विवेक को महत्त्व देना है कि मैं तो निरन्तर रहने वाला हूँ और शरीर मरता न हो। मरने के प्रवाह को ही जीना कहते हैं। वह प्रवाह प्रकट हो जाय तो उसको जन्मना कह देते हैं और अदृश्य हो जाय तो उसको मरना कह देते हैं। तात्पर्य है कि जो हरदम बदलता है, उसी का नाम जन्म है, उसी का नाम स्थिति है और उसी का नाम मृत्यु है। बाल्यवस्था मर जाती है तो वृद्धावस्था पैदा हो जाती है। इस तरह प्रतिक्षण पैदा होने और मरने को ही जीना (स्थिति) कहते हैं। पैदा होने और मरने का यह क्रम सूक्ष्म रीति से निरन्तर चलता रहता है। परन्तु हम स्वयं निरन्तर ज्यों-के-त्यों रहते हैं। अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, पर हमारे स्वरूप में कभी किंचन्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। अतः शरीर तो निरन्तर मृत्यु में रहता है और मैं निरन्तर अमरता में रहता हूँ—इस विवेक को महत्त्व देना है।
गीता में आया है—
मनुष्यतामात्र के भीतर स्वतः यह भाव रहता है कि मैं बना रहूँ, कभी मरूँ नहीं। वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। अगर वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। जैसे, भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु (अन्न और जल) है, जिससे वह भूख-प्यास बुझ जाय। अगर अन्न-जल न होता तो भूख-प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतःसिद्ध है। यहाँ शंका होती है कि जो अमर है, उसमें अमरता की इच्छा क्यों होती है ? इसका समाधान है कि अमर होते हुए भी जब उसने अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्म शरीर के साथ अपने को एक मान लिया अर्थात् ‘शरीर ही मैं हूँ’—ऐसा मान लिया, तब उसमें अमरता की इच्छा और मृत्यु का भय पैदा हो गया।
मनुष्य मात्र को इस बात का विवेक है कि यह शरीर (स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर) मेरा असली स्वरूप नहीं है। शरीर प्रत्यक्ष रूप से बदलता है। बाल्यावस्था में जैसा शरीर था, वैसा आज नहीं है और आज जैसा शरीर है, वैसा आगे नहीं रहेगा। परन्तु मैं वही हूँ अर्थात् बाल्यवस्था में जो मैं था, वही मैं आज हूँ और आगे भी रहूँगा। अतः मैं शरीर से अलग हूँ और शरीर मेरे से अलग है अर्थात् मैं शरीर नहीं हूँ—यह सबके अनुभव की बात है। फिर भी अपने को शरीर से अलग न मानकर शरीर के साथ एक मान लेना अपने विवेक का निरादार है अपमान है, तिरस्कार है। साधक को अपने इस विवेक को महत्त्व देना है कि मैं तो निरन्तर रहने वाला हूँ और शरीर मरता न हो। मरने के प्रवाह को ही जीना कहते हैं। वह प्रवाह प्रकट हो जाय तो उसको जन्मना कह देते हैं और अदृश्य हो जाय तो उसको मरना कह देते हैं। तात्पर्य है कि जो हरदम बदलता है, उसी का नाम जन्म है, उसी का नाम स्थिति है और उसी का नाम मृत्यु है। बाल्यवस्था मर जाती है तो वृद्धावस्था पैदा हो जाती है। इस तरह प्रतिक्षण पैदा होने और मरने को ही जीना (स्थिति) कहते हैं। पैदा होने और मरने का यह क्रम सूक्ष्म रीति से निरन्तर चलता रहता है। परन्तु हम स्वयं निरन्तर ज्यों-के-त्यों रहते हैं। अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, पर हमारे स्वरूप में कभी किंचन्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। अतः शरीर तो निरन्तर मृत्यु में रहता है और मैं निरन्तर अमरता में रहता हूँ—इस विवेक को महत्त्व देना है।
गीता में आया है—
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही।।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही।।
(2। 22)
‘मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नये कपड़े धारण कर
लेता
है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नये शरीरों में चला जाता
है।’
जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नये कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते। तात्पर्य है कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जायँ तो फिर पुण्य-पापका फल कौन भोगेगा ? अन्य योनियों में कौन जायगा ? बन्धन किसका होगा ? मुक्ति किसकी होगी ?
शरीर नाशवान् है, इसको कोई रख सकता ही नहीं और हमारा स्वरूप अवनाशी है, इसको कोई मार सकता ही नहीं—
जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नये कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते। तात्पर्य है कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जायँ तो फिर पुण्य-पापका फल कौन भोगेगा ? अन्य योनियों में कौन जायगा ? बन्धन किसका होगा ? मुक्ति किसकी होगी ?
शरीर नाशवान् है, इसको कोई रख सकता ही नहीं और हमारा स्वरूप अवनाशी है, इसको कोई मार सकता ही नहीं—
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्।
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति।।
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति।।
(गीता 2/17)
अविनाशी सदा अवनाशी ही रहेगा और विनाशी सदा विनाशी ही रहेगा। जो विनाशी
है, वह हमारा स्वरूप नहीं है। हमने कुर्ता पहन लिया तो क्या कुर्ता हमारा
स्वरूप हो गया ? हमने चादर ओढ़ ली तो क्या चादर हमारा स्वरूप हो गयी ?
जैसे हम कपड़ों से अलग हैं ऐसे ही हम इन शरीरों से भी अलग हैं। इसलिए
हमारे मन में निरन्तर स्वतः यह बात रहनी चाहिये कि मैं मरने वाला नहीं
हूँ, मैं तो अमर हूँ। ‘अमर जीव मरे सो काया’ जीव अमर
है, काया
मरती है। अगर इस विवेक को महत्त्व दें तो मरने का भय मिट जायगा। जब हम
मरते ही नहीं तो फिर मरने का भय कैसा ? और जो मरता ही है, उसको रखने की
इच्छा कैसी ? हमारा बालकपना नहीं रहा तो अब हम बालकपने को लाकर नहीं दिखा
सकते ! क्योंकि वह मर गया, पर हम वही रहे। अतः शरीर सदा मरनेवाला है और
मैं सदा अमर रहनेवाला हूँ—इसमें क्या सन्देह रहा ? अब केवल इस
बात
का आदर करना है इसको महत्त्व देना है, इसका स्वयं अनुभव करना है, कोरा
सीखना नहीं है। जैसे धन मिल जाय तो भीतर से खुशी आती है, ऐसे ही इस बात को
सुनकर भीतर से खुशी आनी चाहिये और जीने की इच्छा तथा मरने का भय नहीं रहना
चाहिये ! कारण कि जिस बात से हमारा दुःख, जलन, सन्ताप, रोना मिट जाय, उसके
मिलने से बढ़कर और क्या खुशी की बात होगी ! ऐसा लाभ तो करोड़ों-अरबों
रुपयों के मिलने से भी नहीं होता। कारण कि अरबों-खरबों रुपये मिल जायँ और
पृथ्वी का राज्य मिल जाय तो भी एक दिन वह सब छूट जाएगा, हमारे से बिछुड़
जायगा !
अरब खरब लौं द्रव्य है, उदय अस्त लौं राज।
तुलसी जो निज मरन है, तो आवे किहि काज।।
तुलसी जो निज मरन है, तो आवे किहि काज।।
हम शरीर में अपनी स्थिति मान लेते हैं, अपने को शरीर मान लेते हैं तो यह
हमारी गलती है। गलत बात का आदर करना और सही बात का निरादर करना ही मुक्ति
में खास बाधा है। अपने को शरीर मानकर ही हम कहते हैं कि मैं बालक हूँ, मैं
जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। वास्तव में हम न बालक हुए, न हम जवान हुए, न हम
बूढ़े हुए, प्रत्युत शरीर ही बालक हुआ, शरीर ही जवान हुआ, शरीर ही बूढ़ा
हुआ। शरीर बीमार हो गया तो मैं बीमार हो गया, शरीर कमजोर हो गया मैं कमजोर
हो गया, धन पास में आ गया तो मैं धनी हो गया, धन चला गया तो मैं निर्धन हो
गया—यह शरीर और धन के साथ एकता मानने से ही होता है।। जब क्रोध
आता
है, तब हम कहते हैं कि मैं क्रोधी हूँ ! विचार करें, क्या क्रोध सब समय
रहता है ? सबके लिये होता है ? जो हरदम नहीं रहता और जो सबके लिये नहीं
होता, वह मेरेमें कैसे हुआ ? कुत्ता घर में आ गया तो क्या वह घर का मालिक
हो गया ? ऐसे ही क्रोध आ गया तो क्या मैं क्रोधी हो गया ? क्रोध तो आता है
और चला जाता है, पर मैं निरन्तर रहता हूँ।
|
|||||
विनामूल्य पूर्वावलोकन
Prev
Next
Prev
Next
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i